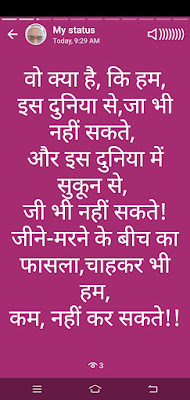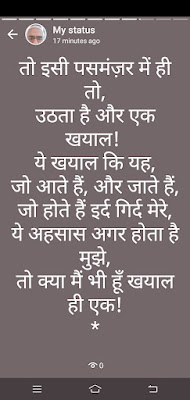अपनी आत्मा के स्वरूप का आविष्कार
---------------------©----------------------
आध्यात्मिक आत्मानुसन्धान के अभ्यास में एक बड़ी कठिनाई यह है कि यद्यपि न तो कोई भी अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ हो सकता है, न होता ही है, क्योंकि हर कोई ही अपनी स्वाभाविक अन्तःप्रेरणा से भी अपने अस्तित्व से अनायास अवगत ही होता है, और स्वयं के होने के सत्य को सदा ही घोषित भी करता ही है, किन्तु स्वरूप की दृष्टि से यह अपना अस्तित्व, 'स्वयं' क्या है इसे जान पाना, कह पाना या अनुभव कर पाना तो अत्यन्त ही कठिन है।
इसलिए विज्ञानात्मा, जिसे 'मध्वदं' कहा जा रहा है, को स्पष्टता से समझने पर आत्मानुसन्धान का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है।
पहले कठोपनिषद् उपनिषद् के अध्याय २, वल्ली प्रथम का यह मंत्र :
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्।।
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते।। एतद्वै तत्।।५।।
पूज्यपाद भगवान् आचार्य शङ्कर ने इस उपनिषद् पर अपने भाष्य में इसका अर्थ "कर्मफलभुज", जीव किया है।
यः कश्चित् इमं मध्वदं = कर्मफलभुजं = जीवं प्राणादि-कलापस्य धारयितारं आत्मानं वेद = विजानाति, अन्तिकात् = अन्तिके = समीपे ईशानम् = ईशितारं भूतभव्यस्य = कालत्रयस्य ततः -तत् -विज्ञानात् ऊर्ध्वं आत्मानं न विजुगुप्सते = न गोपायितुम् इच्छति अभय-प्राप्तत्वात्।
शिव अथर्वशीर्ष मंत्र ६ में रुद्र द्वारा भोगायमान दशा में सृष्टि का सृजन करने के बाद संहरण कर सो जाने के बाद पुनः जाग जाने के अनन्तर सृष्टि का सृजन किए जाने का वर्णन है, और "... ... अर्चयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यद्ध्रुवम् । एतद्धि परमं तपः आपो ज्योति रसोऽमृतं भूर्भुवः स्वरों नम इति।।६।।
इस प्रकार तप से ही सृष्टि का सृजन, पालन पोषण और संहरण होता है।
मध्वदं का अन्वय होगा मधु-अदं, जो :
"अद्" धातु सेवन करने के अर्थ में मधु अर्थात् जो इस सृष्टि का परमोत्कृष्ट फल है, उसका उपभोग करनेवाले जीव का द्योतक है। यही विज्ञानात्मा है इसे भी आचार्य द्वारा स्पष्ट किया ही गया है।
इसकी पुष्टि इन सुप्रसिद्ध मंत्रों से भी होती है :
द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।।६।।
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः।।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।।७।।
(श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय ४)
--
य इमं मध्वदं वेद आत्मानम् जीवम्-अन्तिकात्। ईशानं भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते।। एतत् वै तत्।।
जो इस सुख-दुःख-रूपी कर्मफल का भोग करनेवाले जीवात्मा को ही विज्ञानात्मा के रूप में अपने भीतर विद्यमान, भूत और भव्य परमात्मा की तरह जानता है, वह फिर भी से रहित होकर राग-द्वेष से रहित होकर, शोक से भी रहित हो जाता है।
***